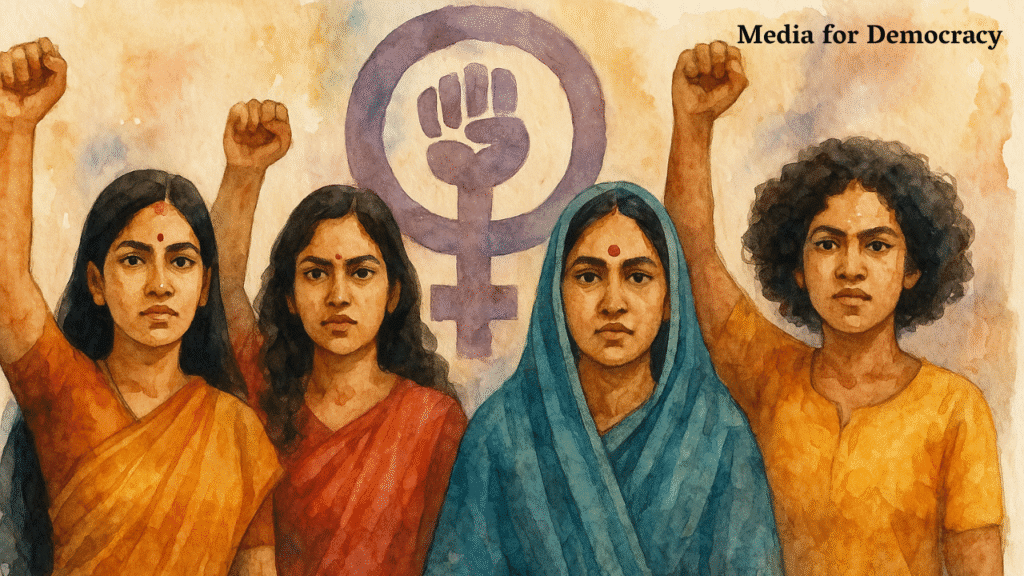प्रीती शुक्ला | ३१ अगस्त २०२५
भारतीय समाज में औरतों के सपनों की कहानी हमेशा अधूरी क्यों रह जाती है? यह सवाल जितना व्यक्तिगत लगता है, उतना ही सामाजिक और राजनीतिक भी है। लड़कियों के जीवन में बचपन से लेकर युवावस्था तक अदृश्य बंदिशों का ऐसा जाल बुन दिया जाता है कि उनके सपनों तक पहुँचने का रास्ता या तो बहुत लंबा हो जाता है या बीच में ही थम जाता है। यह स्थिति केवल ग्रामीण इलाक़ों या परंपरागत परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि महानगरों और शिक्षित वर्गों में भी दिखाई देती है।
बचपन की यादों में हर लड़की कभी न कभी यह सुनती है—“इतनी देर बाहर मत रहो,” “लड़कियाँ ज़्यादा खेलों में भाग नहीं लेतीं।” सुरक्षा और संस्कार के नाम पर खड़ी की गई ये दीवारें धीरे-धीरे उनके आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर कमजोर करने लगती हैं।
मुझे अपनी एक सहेली याद आती है, जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। लेकिन घरवालों का कहना था—“ये तो लड़कों का खेल है।” धीरे-धीरे उसने खेलना छोड़ दिया और मान लिया कि उसके लिए यही सही है। ऐसे अनगिनत सपने बचपन की दहलीज पर ही दम तोड़ देते हैं।
शिक्षा और अधूरी आज़ादी
आज लड़कियाँ उच्च शिक्षा पा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, लेकिन शिक्षा का मक़सद अक्सर नौकरी या आत्मनिर्भरता से ज़्यादा “शादी में अच्छी जोड़ी” बनाना माना जाता है। डिग्री कई बार करियर का पासपोर्ट बनने के बजाय दहेज घटाने का साधन भर रह जाती है।
शिक्षा का असली मक़सद—सोचने की स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपनी पहचान बनाना—पीछे छूट जाता है।
भारत की लाखों लड़कियों की कहानियाँ एक जैसी हैं। बचपन में डॉक्टर, खिलाड़ी, लेखक या अधिकारी बनने का सपना देखने वाली ये पीढ़ी, युवावस्था में शादी, घरेलू ज़िम्मेदारियों और सामाजिक दबावों में अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती है।
समाज अब भी यही मानता है कि औरत की असली पहचान उसकी रिश्तों से है—किसी की बेटी, बहन या पत्नी के रूप में। उसकी अपनी इच्छाएँ और उपलब्धियाँ अक्सर रिश्तों की परतों के नीचे दब जाती हैं।

बदलते दौर की हलचल
फिर भी यह सच है कि हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं। आज की महिलाएँ पहले से अधिक मुखर हैं। वे सवाल पूछ रही हैं, अपनी आवाज़ लिख रही हैं, मंचों पर रख रही हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी बात कहने की ताक़त दी है।
लेकिन सच्चाई यह भी है कि बदलाव अधूरा है। बहुत-सी कामकाजी महिलाएँ दफ़्तर में लंबे घंटे बिताने के बाद घर लौटकर “दूसरी पारी” खेलती हैं—घर का सारा काम भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी माना जाता है। यानी बाहर की आज़ादी मिली, पर भीतर की बेड़ियाँ जस की तस हैं।
औरतों को बराबरी देना कोई उपकार नहीं, यह उनका संवैधानिक और मानवीय हक़ है। परिवार, स्कूल और समाज अगर शुरुआत से ही बेटा-बेटी को समान दृष्टि से देखें, तभी असली बदलाव संभव है।
बराबरी का अर्थ यह है कि औरतें अपनी पढ़ाई, करियर और जीवन के फैसले बिना किसी मंज़ूरी या दबाव के ले सकें। बराबरी घर की चारदीवारी से निकलकर कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन तक पहुँचे।
पुरुषों की भूमिका
महिलाओं की उड़ान में पुरुषों की भूमिका अनदेखी नहीं की जा सकती। एक पिता जब बेटी को सपने देखने देता है, एक भाई जब बहन के साथ खड़ा होता है और एक पति जब पत्नी की सफलता को अपनी जीत मानता है—तो बदलाव की राह और आसान हो जाती है।
यह समझना ज़रूरी है कि महिलाओं की सफलता पुरुषों के लिए ख़तरा नहीं, बल्कि साझा जीत है।
हर लड़की की आँखों में एक आसमान बसता है। कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई लेखक, कोई खिलाड़ी। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन सपनों की खूबसूरती यही है कि वे कभी मरते नहीं, वे सही माहौल और सही समय का इंतज़ार करते हैं।
भारत बदल रहा है, लेकिन यह सफ़र अभी अधूरा है। हर घर में एक लड़की खिड़की से आसमान देखती है और सोचती है—“क्या मैं कभी उड़ पाऊँगी?” हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उसका आसमान सिर्फ ख्वाहिश न रहे, हक़ बन जाए।
आज ज़रूरत इस बात की है कि औरतों के सपनों को “अनुमति” नहीं, बल्कि “अधिकार” समझा जाए। तभी सचमुच कहा जा सकेगा कि औरतों की उड़ान अब आज़ाद है।

प्रीती शुक्ला एक मुक्त पत्रकार (Independent Journalist) हैं, जो समाज और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर लिखती हैं। वह महिलाओं के अनुभवों और उनके संघर्षों को अपनी लेखनी के माध्यम से मुखर करने का काम करती हैं।