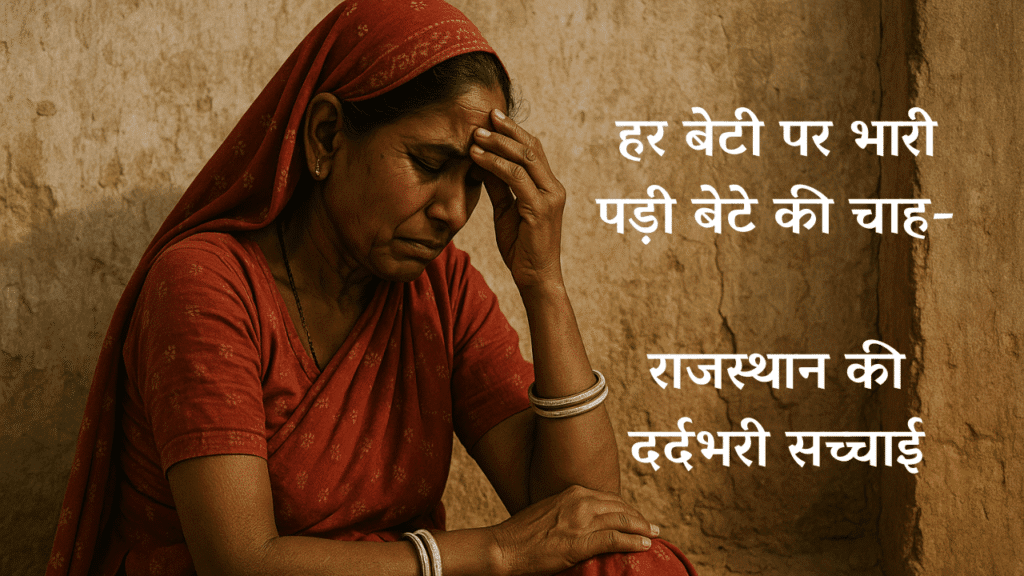यह कहानी है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी ज़िले के पदमपुरा कस्बे के छोटे से गाँव टोडाभीम की। यह कहानी है शीला देवी मीणा की, जिनका जीवन उस सामाजिक सोच का आईना है जिसमें बेटा पैदा करने की चाहत, स्त्री की इच्छाओं और अधिकारों से कहीं ऊपर रखी जाती है। शीला देवी की शादी टोडाभीम के एक सम्पन्न परिवार में हुई। परिवार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उनका बड़ा बेटा सरपंच बने, शीला देवी का विवाह उसी बेटे से कराया गया। यह विवाह पूरी परंपरा के अनुसार हुआ, यहाँ तक कि लड़का और लड़की एक-दूसरे को विवाह से पहले देख तक नहीं पाए थे। शादी के बाद शीला देवी से तुरंत संतान की अपेक्षा की जाने लगी। जब उनकी पहली संतान हुई और वह बेटी थी, तो घरवालों ने इसे दुर्भाग्य माना। उन्हें ताने दिए गए कि बहू एक बेटा भी न दे सकी।
बेटे की चाह में शीला देवी पर फिर से गर्भ धारण करने का दबाव बनाया गया। सामान्यतः दो बच्चों के बीच तीन साल का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ शीला देवी को साल भर भी आराम नहीं दिया गया। यह विडंबना है कि वही माँ, जो बच्चे को जन्म देती है, पालती है और उसके संस्कारों की ज़िम्मेदारी उठाती है, उससे यह तक नहीं पूछा जाता कि वह कब माँ बनना चाहती है। दूसरी बार भी बेटी हुई। अब परिवार के सामने नई समस्या थी—नियमों के अनुसार, यदि दो से अधिक संतानें हों तो पति सरपंच नहीं बन सकता। लेकिन घरवालों का कहना था कि सरपंची का क्या लाभ, अगर बेटा ही न हो जो इस विरासत को आगे बढ़ाए। अंततः तय हुआ कि एक और संतान होगी और सरकारी दस्तावेज़ में बिना जिक्र कियें चुनाव भी लड़ा जाएगा।

अब शीला देवी को तीसरी संतान भी बेटी हुई। अब उन्हें परिवारने “अशुभ” मान लिया। उन्हें घर की खराब किस्मत का दोषी ठहराया गया। उनके साथ गाली-गलोच होने लगी। लेकिन मीणा परिवार का लालच थमा नहीं। शीला मीणा की चौथी और पाँचवीं संतान भी बेटियाँ हुई। इस दौरान शीला देवी की राय का कोई महत्व नहीं था। वह माँ बनने के लिए तैयार हैं या नहीं, यह सवाल कभी पूछा ही नहीं गया। केवल बेटे की चाह ने उन्हें लगातार गर्भवती होने पर मजबूर कर दिया। अंततः छठी संतान के रूप में उनके घर बेटा पैदा हुआ। परिवार को उम्मीद थी कि अब विरासत संभालने वाला वारिस मिल गया। लेकिन सोच वहीं की वहीं रही—“एक बेटा पाँच बहनों का बोझ कैसे उठाएगा? एक और बेटा होना चाहिए।” फिर से शीला देवी की सहमति को नज़रअंदाज़ किया गया। उन्हें एक बार और गर्भवती होना पड़ा। इस बार भी बेटी हुई। अब परिवार में माँ-बाप सहित नौ लोग हो गए।
यह स्थिति केवल मीणा परिवार की नहीं है। भारत जैसे देश में, जहाँ दो बच्चों का पालन-पोषण ही संघर्षपूर्ण है, वहाँ केवल बेटे की उम्मीद में सात संतानें पैदा करना सोचने पर मजबूर करता है।
सरपंच का चुनाव और विडंबना
७ बच्चें भी शीला देवी के पति ने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर उन्हें अपना सरपंच पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि नियम साफ़ था—दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकते। यहाँ तो संख्या सात थी। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद शीला देवी ने हार नहीं मानी। जिन बेटियों को केवल एक बेटे की चाह में इस दुनिया में लाया गया था, उन्हें भी उतना ही प्यार और शिक्षा दी जितना अपने बेटे को। उन्होंने अपनी चार बेटियों की शादी धूमधाम से की और सभी बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया। यह केवल एक माँ का ही साहस हो सकता है, जो सात बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक जैसा बड़ा करे।
महिला अधिकार और संविधान : एक अधूरी लड़ाई
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और अधिकारों पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। लेकिन आज भी यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या महिला को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह तय करे, कब और कितनी बार वह माँ बने? यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि उसकी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दुर्भाग्य से, हमारे समाज में अब भी महिलाओं को बार-बार गर्भधारण के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार परिवार और सामाजिक दबाव के चलते महिलाओं की इच्छा को दरकिनार कर दिया जाता है। यह न केवल उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।

एक और गहरी समस्या यह है कि बेटियों को आज भी “बेटे की अनुपस्थिति” का विकल्प समझा जाता है। समाज की मानसिकता में यह विचार गहराई से बैठा है कि परिवार की वंश परंपरा और पहचान केवल बेटे के माध्यम से ही आगे बढ़ सकती है। बेटियों को इस सोच के चलते अक्सर उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह दृष्टिकोण न केवल महिलाओं को हीन समझता है, बल्कि समानता और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को भी ठेस पहुँचाता है। आज भी बहुत से परिवारों में बेटियों को बोझ या ‘पराया धन’ मानने की प्रवृत्ति बनी हुई है।
भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और गरिमा प्रदान की है।
- अनुच्छेद 14 प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, जिसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
- अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसका अर्थ है कि महिला के शरीर और उसके जीवन पर उसका अपना अधिकार है।
- अनुच्छेद 15(1) स्पष्ट रूप से लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित करता है।
इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, ज़मीनी हकीकत काफी अलग है। महिलाओं के अधिकार अक्सर सामाजिक मान्यताओं, पितृसत्तात्मक सोच और धार्मिक-सांस्कृतिक दबावों की भेंट चढ़ जाते हैं। जब महिलाओं से उनकी मर्ज़ी पूछे बिना माँ बनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह संविधान में दिए गए अधिकारों की खुली अवहेलना है।
समाज को यह समझना होगा कि बेटियाँ किसी भी दृष्टि से बेटों से कम नहीं हैं। बेटियाँ न केवल परिवार की शान होती हैं, बल्कि वे समाज और राष्ट्र निर्माण में भी बराबर का योगदान देती हैं। महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि एक सशक्त और समानतापूर्ण समाज की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
आज समय की मांग है कि हम संवैधानिक मूल्यों को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सामाजिक जीवन में उतारें। महिलाओं को यह स्वतंत्रता मिले कि वे स्वयं तय कर सकें कि उन्हें कब और कितनी बार माँ बनना है। जब तक यह स्वतंत्रता वास्तविक रूप से सुनिश्चित नहीं होती, तब तक महिलाओं के अधिकार अधूरे रहेंगे और समानता का सपना भी अधूरा ही रहेगा।
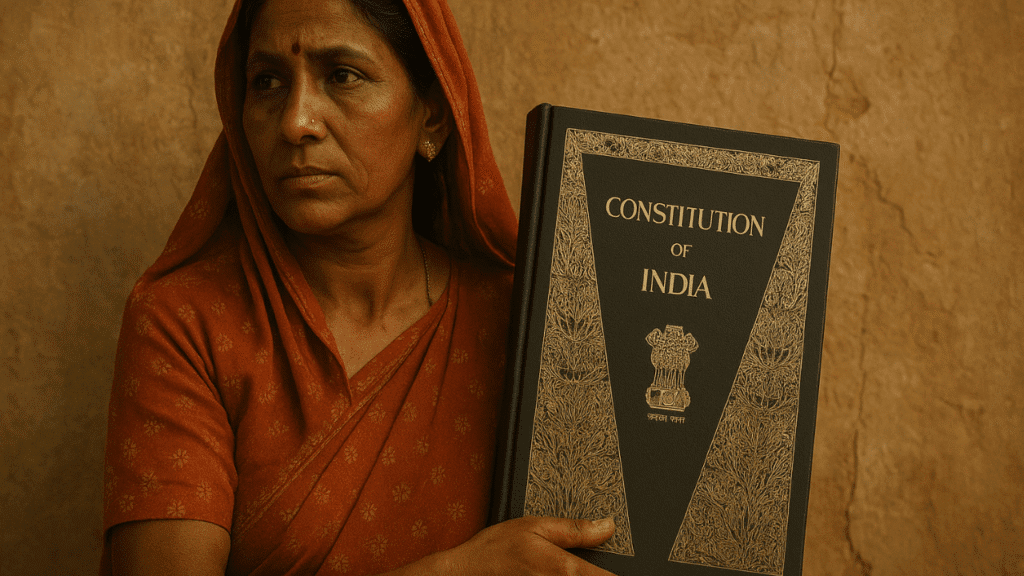
आज के हालात
आज की दुनिया बदल रही है—मौहलात भी, परिवार भी और शहर की सोच भी। लेकिन राजस्थान के कुछ ज़िले आज भी उस पुरानी सोच से पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं, जहाँ बेटियों का अनुपात बेटों से कम है। उदाहरण के तौर पर, करौली जिले में जहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 858 महिलाएँ हैं—जो सावित करता है कि संतानों में अब भी लिंग असंतुलन मौजूद है। शिक्षा का रुख भी कुछ बेहतर नहीं है—राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर लगभग 80%, जबकि महिला साक्षरता मात्र 57.6% है, यानी बीच में 23.2 प्रतिशत की खाई है। यही नहीं—NFHS-5 के अनुसार, 25.4% लड़कियाँ 18 साल के पहले विवाह की शिकार होती हैं—जो ग्रामीण इलाकों में 28.3% तक बढ़ जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 15.1% ही है। फिर भी, सच्चाई यही है—“म्हारी छोरियाँ छोरों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं।” वे हिम्मत, प्रतिभा और क्षमता में जितनी मजबूत हैं, उतनी ही अदम्य हैं। बचपन में पीछे छोड़ दिया जाए, पर समय आने पर वे हर चुनौती सामना कर उच्चाई तक पहुंच सकती हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बेटियाँ भी उतनी ही सक्षम हैं जितने बेटे। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में यह सोच बदलनी होगी कि घर की विरासत केवल बेटा ही आगे बढ़ा सकता है।
विशेषज्ञ दृष्टिकोण : अरुणा रॉय के विचार
महिलाओं के अधिकार और समानता की लड़ाई में अरुणा रॉय का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि “महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष उनकी गरिमा की रक्षा के लिए है।” अरुणा रॉय ने राजस्थान के ग्रामीण इलाक़ों में महिलाओं के साथ गहराई से काम किया है और करीब से देखा है कि किस तरह समाज में महिलाओं को लगातार कमतर आंका जाता है तथा उनके बुनियादी अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं।
उनकी पहल, मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS), न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सफल रही है, बल्कि उन्हें सामाजिक भागीदारी और समान स्थान दिलाने की दिशा में भी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। अरुणा रॉय का मानना है कि समानता केवल कानूनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे समाज और मानसिकता के स्तर पर भी स्थापित करना होगा।

शीला देवी की कहानी इसका ज्वलंत उदाहरण है। बेटे की चाहत में उन्हें बार-बार गर्भवती होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनकी अपनी इच्छाओं और अधिकारों को नज़रअंदाज़ किया गया। यह वही सामाजिक दबाव और मानसिकता है, जिसकी ओर अरुणा रॉय लगातार इशारा करती रही हैं।
अरुणा रॉय के विचार हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि जब तक महिलाएँ अपनी आवाज़ बुलंद कर अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होंगी, तब तक उनकी गरिमा और स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। उनकी दृष्टि इस बात को और स्पष्ट करती है कि समाज में महिलाओं के लिए वास्तविक समानता स्थापित करने के लिए सिर्फ़ संवैधानिक प्रावधान काफ़ी नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सोच और व्यवहार में भी बदलाव लाना ज़रूरी है।
महिलाओं के अधिकार केवल काग़ज़ों पर लिखे संवैधानिक प्रावधान नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन और गरिमा से जुड़े मौलिक तत्व हैं। फिर भी, समाज में बेटों की चाहत, पितृसत्तात्मक सोच और परंपरागत दबाव महिलाओं को अपने ही जीवन पर निर्णय लेने से वंचित कर देते हैं। अरुणा रॉय जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता और समानता दिलाने की लड़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए।
शीला देवी जैसी अनगिनत कहानियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि बदलाव केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक सोच और मानसिकता के परिवर्तन से आएगा। जब तक महिलाएँ अपनी इच्छा से यह तय नहीं कर पाएँगी कि उन्हें कब और कितनी बार माँ बनना है, तब तक समानता का सपना अधूरा रहेगा।
अब समय है कि समाज, परिवार और राज्य – सभी मिलकर महिलाओं की गरिमा और अधिकारों को वास्तविक रूप से स्वीकारें और सुनिश्चित करें। तभी हम उस भारत की ओर बढ़ पाएँगे, जहाँ बेटियों और बेटों के बीच कोई भेदभाव न हो और हर महिला अपने जीवन पर पूरी स्वतंत्रता और नियंत्रण रख सके।
उज्ज्वल उपमन मुंबई विश्वविद्यालय के संचार एवं पत्रकारिता विभाग से जुड़े हैं। वे सामाजिक सरोकारों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं और सशक्तिकरण पर लेखन करते हैं। उनकी लेखनी का उद्देश्य समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाना है।