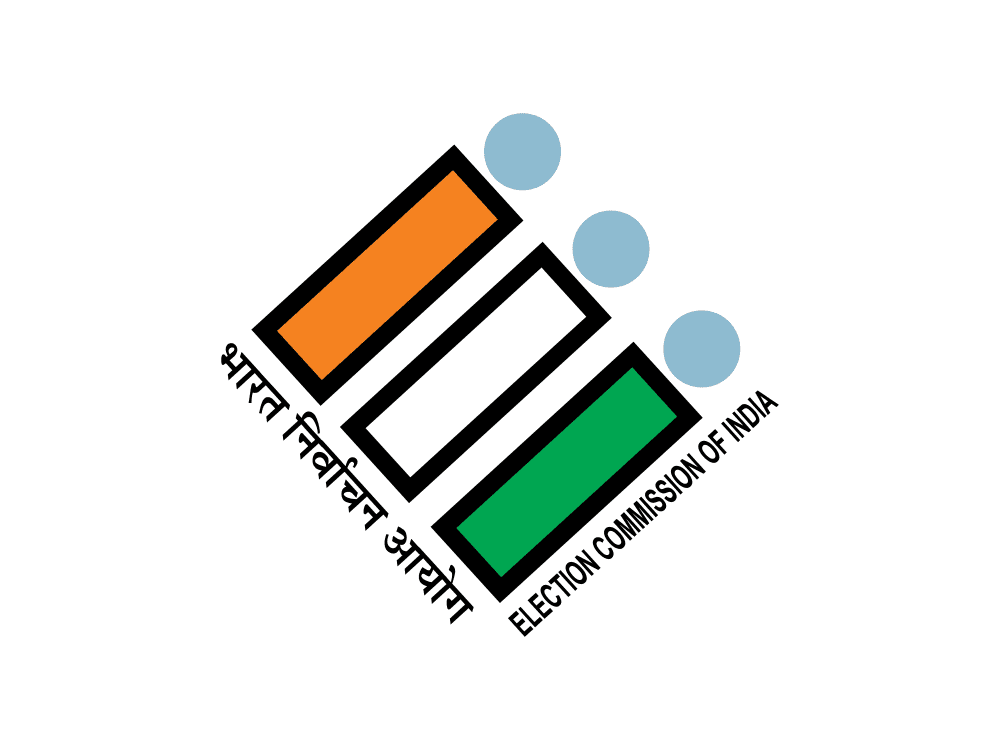डॉ. सागर भालेराव
कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ। मुंबई की सेंट्रल लाइन पर स्थित अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति असंतुलित होकर प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, कुछ ने दौड़कर उसकी मदद की। सौभाग्य से वह व्यक्ति बच गया। लेकिन यह घटना एक सख्त सच्चाई उजागर कर गई — मुंबई की लोकल ट्रेनों का नेटवर्क, जो शहर की जीवनरेखा कहा जाता है, अभी भी दिव्यांगजनों के लिए एक खतरनाक और अपूर्ण प्रणाली है।
यह कोई एकल घटना नहीं थी। यह उस प्रणाली की गवाही है जो रोज़ाना लाखों यात्रियों को तो ढोती है, लेकिन उनमें से जो शारीरिक रूप से अलग तरह से सक्षम हैं, उनके लिए यह प्रणाली मानो कोई बाधा बन जाती है। भारत में कई कानून और योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों को बराबरी का अधिकार देने की बात करती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई अंबरनाथ जैसी घटनाओं में साफ नज़र आती है।
नीतियों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) कहता है कि सार्वजनिक स्थानों को सभी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। सुगम्य भारत अभियान भी इसी दिशा में शुरू किया गया था। लेकिन अंबरनाथ जैसी घटनाएं बताती हैं कि ये कानून अभी तक कागज़ों से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
मुंबई के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट, रैंप और टैक्टाइल टाइलें ज़रूर लगी हैं। कुछ ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कोच भी हैं। लेकिन इन सुविधाओं का दायरा सीमित है और उनका रखरखाव अक्सर खराब रहता है।
अंबरनाथ जैसे स्टेशनों पर न तो प्लेटफॉर्म के किनारे टैक्टाइल संकेत हैं, न ही फुटओवर ब्रिज पर रैंप। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का फासला खतरनाक है। ऑडियो घोषणाएं कई बार अस्पष्ट होती हैं और लिफ्ट अक्सर बंद पड़ी रहती हैं। ट्रेन में आरक्षित कोच तक पहुंचना भीड़भाड़ के कारण बहुत कठिन होता है।
यूनिवर्सल डिज़ाइन: सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए नहीं
अब समय आ गया है कि हम यूनिवर्सल डिज़ाइन (सर्वजन अनुकूल डिज़ाइन) की बात गंभीरता से करें। इसका अर्थ है ऐसी संरचनाएं बनाना जो हर किसी के लिए सहज और सुरक्षित हों, न कि केवल “विशेष” समूहों के लिए।
अगर स्टेशनों में शुरू से ही कम ढलान वाले रैंप, टैक्टाइल संकेत, स्पष्ट दृश्य व श्रव्य घोषणाएं, फिसलन-रहित फर्श और ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बराबर होती — तो अंबरनाथ की घटना शायद नहीं होती। ऐसे डिज़ाइन सिर्फ दृष्टिबाधित या व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं होते, बल्कि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, चोटिल व्यक्तियों और सामान ले जाने वाले यात्रियों के लिए भी सहायक होते हैं।
मीडिया की भूमिका और लोकतंत्र की परीक्षा
अंबरनाथ की घटना की वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया में थोड़ी हलचल मची, लेकिन ये ध्यान अल्पकालिक रहा। मीडिया का दायित्व है कि वह ऐसी घटनाओं को केवल “वायरल क्लिप” तक सीमित न रखे, बल्कि निरंतर पूछे — लिफ्टें काम क्यों नहीं कर रहीं? डिज़ाइन मानकों का पालन क्यों नहीं हो रहा? दिव्यांगजनों की भागीदारी क्यों नहीं हो रही?
जब मीडिया यह मुद्दा दया के बजाय अधिकार के नज़रिए से उठाता है, तब ही असली लोकतांत्रिक बहस जन्म लेती है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की क्षमता एक मौलिक अधिकार है — इसे किसी भी रूप में बाधित करना लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुँचाता है।
अब क्या किया जाना चाहिए?
रेलवे प्रशासन को तुरंत सख़्त कदम उठाने होंगे। प्रत्येक स्टेशन का सुगमता ऑडिट हो, Universal Design के अनुसार पुनर्निर्माण हो, और दिव्यांगजनों को योजना, क्रियान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सुविधा देने के बाद उसके रखरखाव और निगरानी पर भी उतना ही ज़ोर दिया जाए।
अंबरनाथ की घटना एक चेतावनी थी। अगली बार हम उतने भाग्यशाली नहीं भी हो सकते।
मुंबई को अक्सर “शहर जो कभी रुकता नहीं” कहा जाता है। लेकिन अगर ये शहर उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जो दौड़ नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते या देख नहीं सकते — तो हम विकास नहीं कर रहे, हम भेदभाव को स्थायी बना रहे हैं।
सुगमता कोई विशेष सुविधा नहीं, एक मौलिक अधिकार है। और जब तक हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक न तो हमारी ट्रेनें सुरक्षित होंगी, न हमारा लोकतंत्र संपूर्ण।