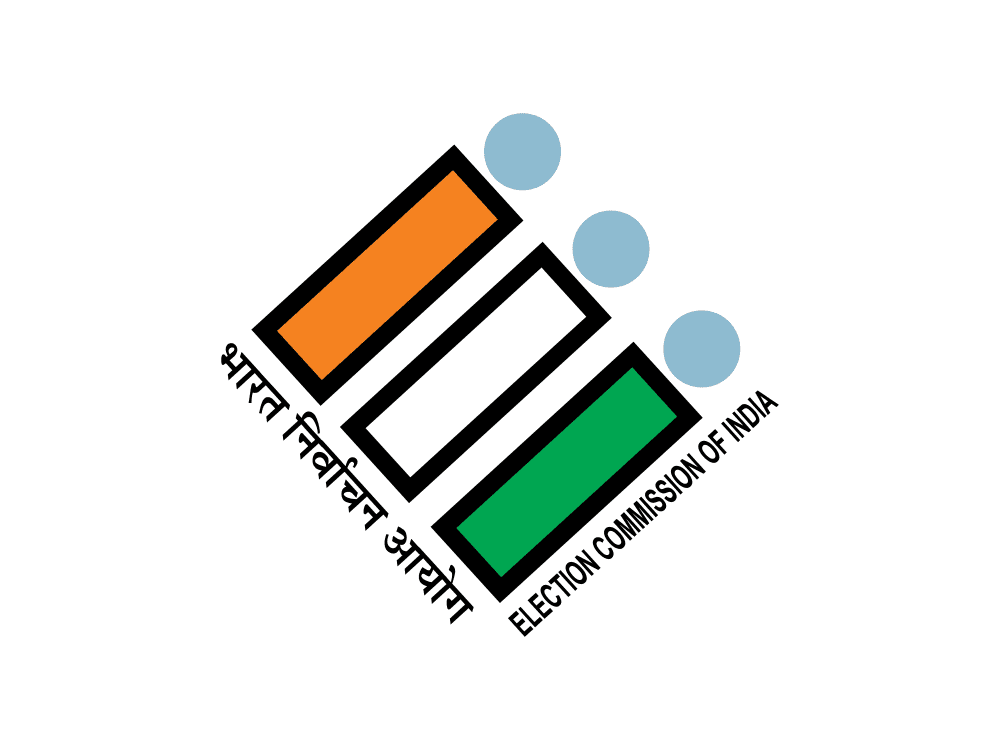उज्ज्वल उपमन | 19 अगस्त 2025
राजस्थान के भरतपुर ज़िले का छोटा सा गाँव — बरौली। धूलभरी गलियों, खेतों की सरसराती फसलों और कुओं से पानी भरती महिलाओं के बीच, एक साधारण-सी कच्ची पक्की दीवारों वाला घर है। इसी घर में रहती हैं रीना जी, अपने पति और छोटे बेटे के साथ। देखने में उनका परिवार किसी सामान्य ग्रामीण परिवार जैसा ही लगता है, लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी है जो धोखे, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
शादी का झूठा सपना
कुछ साल पहले, जब रीना जी की शादी की बात चली, तो उनके परिवार के पास एक रिश्ता आया। लड़के के दादा और पिता दोनों ही शिक्षक रहे, प्रस्ताव लेकर पहुँचे। उन्होंने दावा किया कि लड़का वकील है, एल.एल.बी. की डिग्री ले चुका है और प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि रीना जी उनकी बहू बनकर हमेशा खुश रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने मोटे दहेज की भी माँग रखी।
रीना जी के पिता, जो सीधे-साधे और भरोसा करने वाले इंसान थे, उनकी बातों पर यक़ीन कर लिया। उस समय गाँव में किसी की असलियत जानने के ज्यादा साधन भी नहीं थे। शादी तय हुई, दहेज दिया गया और रीना जी को इस उम्मीद के साथ विदा कर दिया गया कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल होगी।
गाँव वालों की हैरानी
जब बारात बरौली पहुँची और शादी की रस्में पूरी हुईं, तो गाँव के लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें हैरानी थी कि एक बेरोज़गार लड़के को इतना दहेज कैसे मिला। असलियत यह थी कि लड़के वालों ने अपने करीबी रिश्तेदारों से भी सच्चाई छुपा रखी थी। सब कुछ इस तरह पेश किया गया मानो यह रिश्ता पूरी ईमानदारी से हुआ हो।
सच्चाई से सामना
शादी के बाद शुरुआती दिनों में रीना जी ने चुपचाप घर के कामकाज और परंपराओं में खुद को ढाल लिया। गाँव में नई बहू के लिए यह आम बात है कि वह अपने पति या ससुराल वालों से सीधे सवाल न करे। लेकिन समय बीतने के साथ एक बात साफ़ होती जा रही थी की उनका पति न तो कहीं काम पर जाता है और न ही वकालत करता है।
आख़िरकार, एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया। जवाब सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई — पति के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई काम नहीं था और वह पूरी तरह अपने पिता की तनख्वाह और दादा की पेंशन पर निर्भर था। यह शादी केवल इसलिए रचाई गई थी ताकि गाँव वालों को दिखाया जा सके कि उनका बेटा भी शादी कर सकता है, वह भी मोटे दहेज के साथ।
पिता से उम्मीद, लेकिन…
रीना जी ने तुरंत यह बात अपने पिता को बताई। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे उन्हें घर बुला लेंगे और इस धोखाधड़ी से उनका रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। पिता ने कहा, “अब जो हो गया है, सो हो गया है। तुम्हें घर बुलाकर मैं परिवार की इज़्ज़त पर दाग़ नहीं लगा सकता। अब तुम्हें इसी पति के सहारे ज़िंदगी निकालनी होगी।”
उनके लिए यह दूसरा बड़ा झटका था। अब उन्हें समझ आ गया कि वे इस रिश्ते में फँस चुकी हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
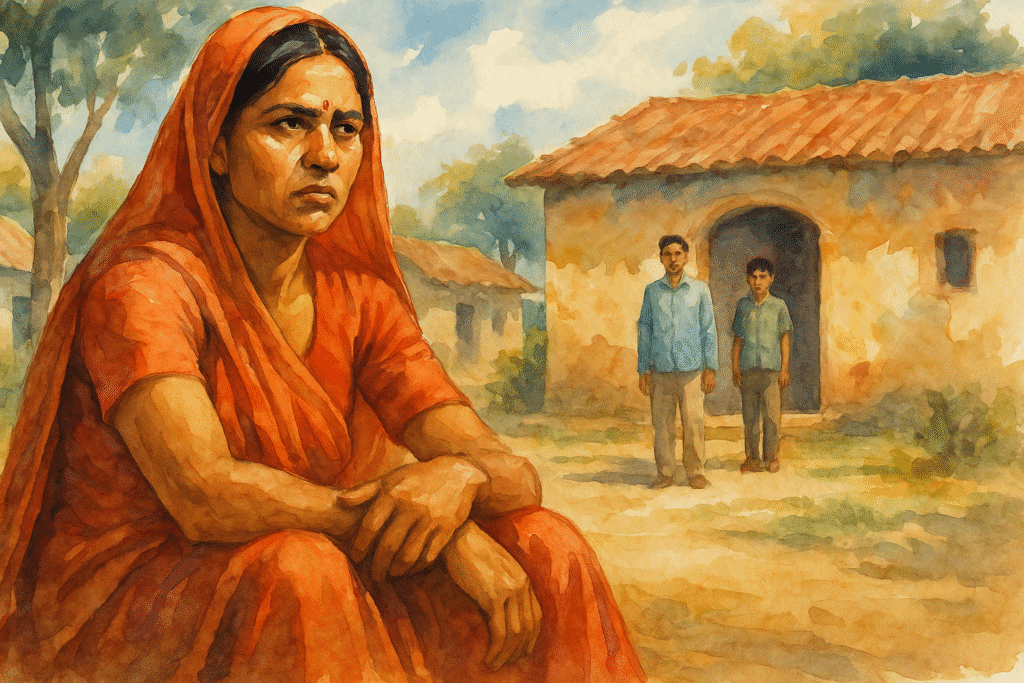
खामोशी का बोझ
ससुराल वालों ने भी यह मान लिया कि रीना जी का मायका उन्हें वापस नहीं बुलाएगा। उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि यह सच्चाई किसी को न बताई जाए। समय बीता और रीना जी गर्भवती हो गईं।
यह फैसला उनका नहीं था — जैसे आज भी देश के कई ग्रामीण इलाकों में होता है, बच्चे पैदा करने का निर्णय पति या ससुराल वालों के हाथ में होता है। जो औरत बच्चा पैदा कर रही है, उसकी राय को महत्व देना ज़रूरी नहीं समझा जाता। अगर वह कुछ कह भी दे, तो घर की बड़ी महिलाएँ ही उसे फटकारकर चुप करा देती हैं और रसोई में भेज देती हैं।
अपने पैरों पर खड़े होने का सफ़र
बेटे के जन्म के बाद ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गईं। रीना जी जानती थीं कि उनके पति इतने सक्षम नहीं कि बेटे को अपनी कमाई से पाल सकें। इसलिए उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया — कभी बुवाई, कभी कटाई, तो कभी चारे की ढुलाई। मेहनत कठिन थी, लेकिन कमाई अपनी थी और उस पर उनका पूरा हक़ था।
धीरे-धीरे यह बात उनके पति को चुभने लगी। उन्होंने कहा कि वे पत्नी की कमाई का खाना नहीं खाएँगे। शायद यह उनकी अहम की बात थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने पिता से खेती का काम सीखना शुरू कर दिया। अब वे भी कुछ कमाने लगे।
शुरुआत में रीना जी की राय घर में कोई नहीं सुनता था। अगर वे किसी घरेलू फैसले में बोलने की कोशिश करतीं, तो घर की बड़ी महिलाएँ ही उन्हें चुप करा देतीं और चाय बनाने को कह देतीं। लेकिन वक्त के साथ, अपनी मेहनत और अडिग इरादे से, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे परिवार की जिम्मेदारियाँ उठा सकती हैं। अब उनकी राय को अनसुना करना आसान नहीं है।
आज की रीना जी
आज रीना जी अपने पति और बेटे के साथ बरौली में ही रहती हैं। वे खेतों में काम करती हैं, घर संभालती हैं और आत्मनिर्भर जीवन जीती हैं। धोखे से शुरू हुई उनकी शादी अब मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और मेहनत की पहचान बन चुकी है।
वे कहती हैं, “अगर मेरे पास 10 रुपये भी हैं, तो मुझे पता है कि मैंने उन्हें अपनी मेहनत से कमाया है।”
रीना जी की कहानी अनोखी नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कई महिलाएँ ऐसे ही हालात झेल रही हैं — कम उम्र में शादी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव, आर्थिक निर्भरता और आवाज़ को दबा देने वाली परंपराएँ। फर्क बस इतना है कि रीना जी ने धीरे-धीरे, चुपचाप, लेकिन मजबूती से अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद संभाल ली
शाम के समय, खेत से लौटकर वे अपने घर के आँगन में बैठती हैं और अपने बेटे को पढ़ते हुए देखती हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि बेटा पढ़-लिखकर बड़ा इंसान बने, लेकिन उससे भी ज़रूरी — वह अपनी पत्नी की राय और सम्मान को अहमियत दे।
“मैं नहीं चाहती कि मेरी कहानी दोहराई जाए,” वे कहती हैं।
संवैधानिक अधिकार और महिलाओं की आवाज़
रीना जी की यह दास्तान हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण इलाक़ों की महिलाएँ अपने जीवन के महत्वपूर्ण फ़ैसले खुद क्यों नहीं ले पातीं। भारतीय संविधान हर नागरिक को बराबरी और सम्मान का हक़ देता है।
- अनुच्छेद 14 – सभी नागरिकों को समानता का अधिकार।
- अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही।
- अनुच्छेद 21 – गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) और घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) – महिलाओं और बच्चियों को शोषण से बचाने के लिए बने क़ानून।
लेकिन हक़ीक़त यह है कि क़ानून किताबों में रह जाते हैं और ज़मीन पर महिलाएँ अब भी झूठ, धोखे और दबाव में जीने को मजबूर हैं।
रीना जी ने अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता से यह साबित किया कि एक महिला जब आर्थिक रूप से मज़बूत होती है, तो उसकी आवाज़ भी सुनी जाने लगती है। लेकिन क्या यह जिम्मेदारी केवल हर महिला पर डाल देना न्यायसंगत है? ज़रूरत इस बात की है कि समाज और क़ानून दोनों मिलकर ऐसे हालात ही न बनने दें।
हमारी ज़िम्मेदारी
इस कहानी का मक़सद केवल सहानुभूति जगाना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि हमें ग्रामीण महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए आवाज़ उठानी होगी। बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। विवाह और मातृत्व जैसे फैसले महिलाओं की सहमति से हों। पंचायत और ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो।
रीना जी की कहानी संघर्ष और जीत की मिसाल है, लेकिन असली जीत तब होगी जब बरौली जैसे गाँवों की हर महिला बिना डर और दबाव के अपने जीवन के फैसले खुद ले सके।
उज्ज्वल उपमन मुंबई विश्वविद्यालय के संचार एवं पत्रकारिता विभाग से जुड़े हैं। वे सामाजिक सरोकारों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं और सशक्तिकरण पर लेखन करते हैं। उनकी लेखनी का उद्देश्य समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाना है।