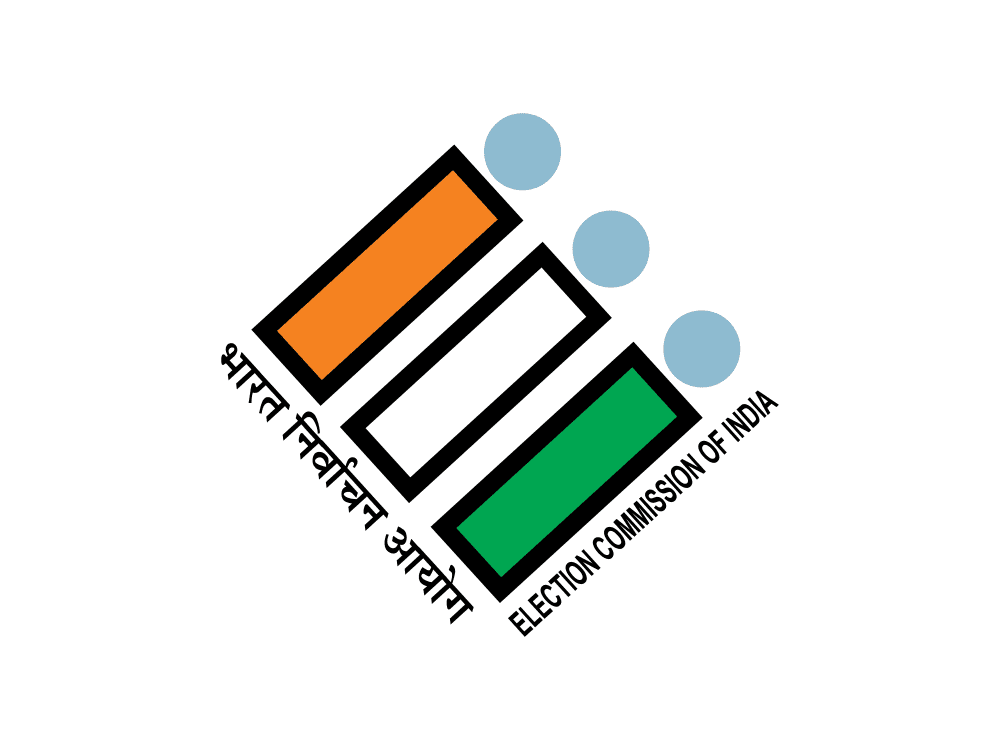रविंद्र मुंडेतिया | 29 अक्तूबर 2025
वैसे तो पहाड़ कई तरह के होते हैं — रेत का पहाड़, बर्फ का पहाड़, उम्मीदों का पहाड़ और कभी-कभी जरूरतों का पहाड़। लेकिन आज हम जिस पहाड़ की बात करने जा रहे हैं, वह कई लोगों की जरूरतों का पहाड़ है। मुंबई की तेज़ रफ़्तार वाली ज़िंदगी को संभालने के लिए हर दिन शहर से हज़ारों टन कचरा ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है। यह कचरा जाकर गिरता है एशिया के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड में, जिसका नाम है देवनार डंपिंग ग्राउंड। यह पहाड़ इतना बड़ा है कि इसकी बदबू और धुआं पूरे इलाके को घेर लेते हैं। लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि इसी बदबू और गंदगी की वजह से कुछ लोगों का घर भी चलता है।
मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड के किनारे सुबह की हवा में नमी कम, बदबू और कभी-कभी धुआं ज़्यादा होता है। दूर-दूर तक कूड़े के पहाड़, काँव-काँव करते कौवे, चीखती हुई ट्रकों की ब्रेक और प्लास्टिक के जलने की तीखी गंध — बस यही इस इलाके की रोज़मर्रा की सुबह है। मैं बात कर रहा हूँ डंपिंग ग्राउंड के पास बसे रफीक नगर की। कच्ची गलियों में बच्चे स्कूल की कॉपी को थैले में छुपाए, नाक पर गमछा बांधकर निकलते हैं, और बड़े लोग हाथ में टिन के डिब्बे और पुराने बोरे लिए उस मैदान की ओर बढ़ते हैं, जिसे शहर ‘डंपिंग ग्राउंड’ कहता है, और ये लोग ‘रोज़गार’।
बस्ती में घुसते ही टीन-टप्पर और तिरपाल से ढके छोटे-छोटे घरों की कतार दिखती है। गलियां सकरी हैं और पानी के निकास के लिए बनी नालियां बिल्कुल जाम हो चुकी हैं। दिन का समय होने के बावजूद गली में कीचड़ है — तो सोचिए सुबह का हाल क्या होता होगा। गली से बाहर निकलते ही सामने देवनार डंपिंग ग्राउंड दिखता है। ऐसा लगा जैसे कचरे का यह पहाड़ मेरी छाती पर लाकर किसी ने रख दिया हो।
एक मोड़ पर, हथेली पर पुराने घावों के निशान लिए, मुझे फातिमा (बदला हुआ नाम) मिलती हैं। बातचीत में पता चला कि फातिमा पिछले 30 सालों से यही रहती हैं और 15 सालों से रैगपिकर का काम कर रही हैं। उम्र है 41 वर्ष। उनसे लंबी बातचीत हुई, और इस दौरान मैंने उनके चेहरे पर कभी ग़म देखा तो कभी खुशी। वे अपने काम को लेकर इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे कहती हैं, “अगर हमें कोई दूसरा काम मिल जाता है, तो आज ही इसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन मुझ जैसी अनपढ़ को काम मिलता भी कहाँ है?”

उस दोपहर मैंने तीन रैगपिकर्स — फातिमा, चंदा और निदा — से लंबी बातचीत की। तीनों के चेहरे पर अलग-अलग कहानियां थीं, लेकिन उनकी परेशानियों का रंग लगभग एक-सा।
फातिमा – चिल्लर के दिनों की बड़ी गिनती
फातिमा के दो बच्चे हैं। दोनों स्कूल जाते हैं। फातिमा बच्चों को डंपिंग ग्राउंड के नजदीक भी नहीं जाने देती हैं। उनका सपना है कि उनके दोनों बच्चे पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी करें। उनके पति के निधन को पांच-छह साल हो चुके हैं। वे सुबह पांच बजे बोरा लेकर निकलती हैं और दोपहर तक प्लास्टिक, टिन, बोतल के ढक्कन, कार्डबोर्ड और कभी-कभार मिलने वाले धातु के टुकड़े अलग-अलग थैलों में भरती हैं।
वे बताती हैं — “प्लास्टिक का रेट 10 से 15 रुपये किलो, गत्ता 5-8 रुपये किलो, और लोहे-पीतल का कुछ अच्छा मिल जाए तो 25-40 रुपये किलो मिल जाते हैं। रोज़ की कमाई 350 से 400 रुपये के बीच होती है। बरसात में गीला कचरा भारी लगता है, पर पैसे वही। कभी-कभी 200 भी नहीं बनते।”
उनके हाथों में छोटे-छोटे कट हैं — कांच और सुइयों से लगे। “दस्ताने मिलते भी हैं तो दो दिन में छिल जाते हैं। कभी-कभी कचरा चुगते वक्त मेडिकल की सुइयां हाथ में लग जाती हैं। खांसी तो जैसे साथी है। रात को सांस फूले तो गरम पानी से भाप लेती हूँ।” डॉक्टर के पास जाना उनके लिए इमरजेंसी का काम है। सामान्य दिनों में दवा की दुकान से 10-20 रुपये की गोली ही इलाज है।
“दो महीने पहले बुखार ऐसा चढ़ा कि तीन दिन तक काम नहीं कर पाई। घर में पैसे कम होते दिखे तो उठकर जाना ही पड़ा।” यह कहते हुए उनके चेहरे पर एक हँसी आई, जो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी।
फातिमा का घर 8×10 का छोटा-सा कमरा है, जो टीन की छत और ईंटों की दीवारों से बना है। बारिश में टपकती बूंदें और कोने में रखा हुआ एक चूल्हा-स्टोव। “बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, पर धुआं और बुखार के दिनों में वो भी नहीं जा पाते।”

चंदा – सांस और आंकड़ों के बीच
चंदा पैंतीस वर्ष की हैं। छह साल पहले मराठवाड़ा से यहां आई थीं। पति पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी करते थे, अब अनियमित काम मिलता है। घर का बड़ा हिस्सा चंदा के कंधों पर है।
“सुबह छह से दोपहर एक तक कचरे के मैदान में रहती हूँ। कई बार तो बीएमसी वाले अंदर जाने भी नहीं देते हैं। आजकल धुएं से आंखें जलती हैं। डॉक्टर ने कहा ‘दमा का शुरुआती लक्षण’ है। इनहेलर महंगा पड़ता है, 400-500 यहीं चले जाते हैं।”
चंदा बताती हैं — “कचरे में अगर लोहे का टुकड़ा मिल जाए तो दिन बन जाता है।” वह हंसते हुए कहती हैं, “पर तौल में अक्सर घटता है। तराज़ू हमेशा खरीदने वाले के पक्ष में होता है। बीच-बीच में सुरक्षा वालों को समझाने की मजबूरी अलग है। कहते हैं, यहां मत जाओ, उधर जाओ। हम भी झगड़ा क्यों करें, थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है।”
बरसात और गर्मियों में बीमारियां बढ़ जाती हैं — त्वचा पर दाग, पेट के संक्रमण, पीठ दर्द, मलेरिया। “कचरे में जो सड़ा-गला होता है, उससे बदबू और मक्खियां आती हैं।” चंदा के घर के सामने नाली खुली रहती है, रात में चूहे दौड़ते हैं। जब उन्होंने अपनी बेटी की बात कही, तो उनकी समस्या और गहरी महसूस हुई।
“मेरी बेटी सातवीं में है। कहती है — माँ, यहाँ बदबू आती है, मैं पढ़ नहीं पाती। पर कहाँ जाएं?”
मैं उनके घर के बाहर कीचड़ से भरी खुली नाली को देखने लगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी मुसीबत बनी हुई है।

निदा – नई उम्र, पुराना काम
निदा बाईस वर्ष की है। चेहरे पर उजली हिम्मत और हाथ में मोटा चुंबक, जिससे वह लोहे के टुकड़े जल्दी ढूंढ लेती है। “डंपिंग ग्राउंड में सबकी अपनी-अपनी नजर और किस्मत होती है। कभी-कभी खुदा किसी पर इतना मेहरबान होता है कि कचरे में से भी अच्छी चीज़ मिल जाती है।”
निदा रोज़ाना 12-15 किलो सामान इकट्ठा कर लेती है। औसतन 300 रुपये बन जाते हैं। कभी-कभार 450 भी। महीने के अंत में 7-8 हजार हाथ में आ जाते हैं, लेकिन किराया, गैस, दवा और घर की जरूरतें निकालकर हाथ में कुछ ही सिक्के बचते हैं।
अपने सपनों के बारे में निदा कहती है — “सिलाई मशीन लेना चाहती हूँ। क्योंकि ये काम बीमारियों का घर है। कभी-कभी बदबू से सिर दर्द करने लगता है तो कभी हाथों में नुकीली चीजें चुभ जाती हैं। सिलाई मशीन ले लूंगी तो कपड़े सिलती रहूंगी।”
निदा को अक्सर आंखों में जलन और सिरदर्द रहता है। उसने अपने दुपट्टे को मास्क की तरह बांधना सीख लिया है, पर असली मास्क और मजबूत दस्ताने दुर्लभ मेहमान हैं।

अगर सरकार यह काम बंद कर दे तो…
जब मैंने फातिमा, चंदा और निदा से पूछा कि अगर सरकार इस डंपिंग ग्राउंड को बंद कर दे या कचरा बीनने वालों को अंदर जाने से मना कर दे, तो वे क्या करेंगीं?
तीनों ने लगभग एक जैसी प्रतिक्रिया दी — “अगर सरकार ऐसा करती है तो पहले हमें रोजगार दे। यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग ये काम करते हैं। लेकिन सरकार को हम जानते हैं — जो आज तक गली की नाली ठीक नहीं करा पाई, वो रोजगार क्या ही देगी।”
इलाके की रोज़मर्रा की जद्दोजहद
डंपिंग ग्राउंड के नजदीक होने का मतलब सिर्फ बदबू नहीं है। यहां रात को भी ट्रक आते-जाते रहते हैं, सायरन बजता है, और कई बार कचरे में आग लगने से धुआं घना हो जाता है। रात भर खिड़की बंद रखो तो दम घुटता है, खोलो तो धुआं अंदर। बरसात में कूड़े का रिसाव, मिट्टी में घुली बदबू और कीचड़ मिलकर काले पानी में बदल जाती है, जो गलियों में बहता है।
सरकारी अस्पताल है, पर कतार लंबी और वक्त कम। प्राइवेट क्लिनिक का मतलब जेब खाली। कभी-कभी टीका लग जाता है, हेल्थ कैंप लगते हैं, पर नियमित इलाज — वह तो एक सपना है।

काम का तंत्र और पैसे की गिनती
रैगपिकर्स का दिन एक अदृश्य अर्थव्यवस्था में गुजरता है। सुबह-सुबह ‘ताजा’ डंपिंग स्पॉट पकड़ना मायने रखता है। जो पहले पहुंचा, उसकी किस्मत मजबूत। फिर शुरू होती है बारीक छटाई — प्लास्टिक को मोटाई से अलग, कागज को सूखे-गीले से, धातु को चुंबक और आवाज़ से। दोपहर होते-होते बोरे भर जाते हैं और फिर पास के कबाड़ी अड्डे पर तौल।
तौल में अक्सर बहस होती है — “अरे इतना कम कैसे? कल तो ज्यादा दिया था!” पर अंततः पैसा उसी तराज़ू से निकलता है।
अच्छे दिनों में कबाड़ी को धातु ज्यादा जाए तो ‘बोनस डे’, वरना बुरे दिनों में खाली बोरा और थकी देह। बीच-बीच में पुलिसिया पूछताछ, सुरक्षा वालों की मनाही, और डंपिंग के अंदर ‘किधर जाओ, किधर नहीं’ का अपना अनलिखा नियम।
“हम लोग कचरा साफ करते हैं,” फातिमा के स्वर में ठहराव आता है, “शहर के लाखों किलो का… पर हमें ही गंदा कहा जाता है।”
बीमारियां, जिनका इलाज वक्त से पहले खुद ही लिखना पड़ता है
कचरा बीनना शरीर पर धीरे-धीरे असर डालता है। सबसे पहले सांस की समस्या, फिर त्वचा में फोड़े-फुंसियां और एलर्जी। पेट में संक्रमण, दस्त, भूख न लगना — आम बातें हैं। महिलाओं के लिए अतिरिक्त चुनौतियां हैं — मासिक धर्म के दिनों में साफ-सफाई, पानी और प्राइवेसी की कमी, बार-बार होने वाले मूत्र संक्रमण।

घर, जो दीवार से ज्यादा ढाल हैं
इन्हें ‘झुग्गी’ कह देना आसान है, पर इन घरों के भीतर ही इनके सपनों की अलमारी, बच्चों की कॉपी-किताबें और दीवार पर टंगे कैलेंडर में त्योहारों की उम्मीदें टंगी होती हैं। फातिमा के घर में दीवार पर बच्चों का बनाया रंगीन घर है, जिसमें धुआं नहीं है। चंदा के घर में लोहे की पेटी है, जिसमें दवा की शीशी और थोड़ी बचत रखी है।
देवनार के पास बसने का मतलब है रोज़गार के पास रहना। पर इसके साथ आती हैं तीखी गंध, धुआं, गंदा पानी, मच्छर और बच्चों के लिए असुरक्षित रास्ते। कई परिवार जगह-जगह से आए हैं — मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक से। रोज़गार के नाम पर शहर में टिके हैं। कागज़-पत्र पूरे नहीं हैं, इसलिए राशन, स्कूल और अस्पताल तक पहुंच भी आधी-अधूरी है।

शहर की सांस और उनके फेफड़े
शहर हर दिन हजारों टन कचरा पैदा करता है। उसमें से जो रिसाइकिल होकर दोबारा शहर में लौटता है, उसमें इन रैगपिकर्स की बड़ी हिस्सेदारी है। वे ऐसी चीजें उठाते-छांटते हैं जिनसे शहर अपना बोझ कम करता है। लेकिन शहर की उजली इमारतों तक उनकी कहानी बहुत कम पहुंचती है।
जब कोई पूछता है — “दिन भर में कितना कमा लेती हो?”, तो जवाब के पीछे एक पूरा दिन का पसीना, धुआं, धूप और छिलते दस्ताने का दर्द छुपा होता है।
यह शहर उनके बिना कल्पना नहीं कर सकता। वे कूड़े में से शहर के लिए कच्चा माल निकालते हैं। लेकिन शहर उनके लिए क्या कर सकता है?
एक सुरक्षित मास्क, दस्ताने, पहचान का कागज़, बच्चों के लिए स्वच्छ हवा और इलाज के लिए खुला दरवाज़ा — शायद इतना कर पाना ही हमारे ‘साफ’ शहर की असल सफाई होगी।
रविंद्र मुंडेतिया मीडिया शोधकर्ता और लेखक हैं। समाज, राजनीति और शहरी मुद्दों पर गहन अध्ययन और लेखन करना उनका मुख्य कार्यक्षेत्र है। वे विशेष रूप से हाशिए पर खड़े समुदायों और पर्यावरणीय चुनौतियों को आवाज़ देने का काम करते हैं।